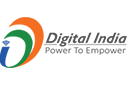उत्तराखंड राज्य में लगातार भूगर्भीय जल के बढ़ते उपयोग एवं उनके अनियोजित दोहन होने तथा प्र्याप्त सम्भरण (रिचार्ज) न होने के कारण भूगर्भीय जल स्तर का लगातार हास्र हो रहा है। राज्य के 13 जिलों में से 11 जिलों का अधिकांष भूभाग पर्वतीय है। वहां पर भी नदी नालों एवं श्रोतों पर लगातार पेयजल एवं सिंचाई आदि की योजनाएं बनायी जा रही है तथा श्रोतों के (रिचार्ज) लिए कोई योजना न होने के कारण श्रोतों के श्राव में कमी देखी जा रही है एवं कतिपय श्रोतों के सूखने की सूचना है। राज्य के औद्योगिकीकरण की बढ़ती सम्भवनाओं को देखते हुए भविष्य में भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने को भी सम्भावना है। यहां जल की प्रचूरता होने के बावजूद पेयजल एवं सिंचाई आदि के लिए पानी की हमेशा कमी रही है। भूगर्भीय जल के स्तर में गिरावट तथा पर्वतीय जनपदों के नदी, नालों एवं श्रोतों के श्राव में कमी को दूर करने के लिए प्रदूषण को नियन्त्रित करने, पेयजल, सिंचाई तथा उद्योग आदि के लिए पानी का सुनियोजित उपयोग आवश्यक है।
उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व पूर्ववर्ती राज्य उत्तर-प्रदेश में ‘‘भूगर्भ जल विभाग‘‘ पृथक रूप से अस्तित्व में था। उत्तरांचल राज्य के मैदानी क्षेत्रों की भूमिगत जल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति इस विभाग द्वारा की जाती थी। इसके लिए मैदानी क्षेत्रों में कई भू-जलस्तर मापक यन्त्र/स्थल तथा वर्षा जल मापक यन्त्र/स्थल स्थापित है, जिनसे आंकड़े एकत्रित कर उपयोग किये जाते हैं। उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आने के बाद इस कार्य हेतु कोई संस्था/विभाग नहीं रह गया था तथा उत्तर प्रदेश द्वारा भी उत्तरांचल क्षेत्र में भूगर्भ जल सम्बन्धी कार्य छोड़ दिया गया है, जिसकमे कारण भूमिगत जल सम्बन्धी आंकडे वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। वैसे भी उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित स्थल अच्छे आंकड़ों के लिए प्र्याप्त नहीं थे, जिसके लिए अतिरिक्त स्टेशन लगाये जाने एवं कर्मचारी लगाये जाने की आवश्यकता होगी। उत्तरांचल के मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों जहां पर नदी नालों एवं श्रोतों के श्राव लगातार कम होते जा रहे हैं, के आंकड़े एकत्र करने के बारे में पूर्व में भी कोई व्यवस्था नहीं थी। समय आ गया है कि उन क्षेत्रों के जलश्राव के हास्र के कारणों को ज्ञात किया जाये। जगह-जगह पर श्रोतों को चिन्हित कर उसके श्राव का मापन किया जाये तथा तुलनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष कर पहुंचा जाये। नदी नालों पर पेड़ झाडियों से पानी को कृत्रिम रूप से रोकने, तथा चाल खाल को संरक्षित करने की जानकारी जनता को बखूबी थी। वर्तमान में यह प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है। चाल खाल नष्ट होते जा रहे हैं। नदी नालों के बहाव को जगह-जगह पर रोककर त्मबींतहम करने की कोई व्यवस्था नहीं रह गयी थी। ऐसे में यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम आंकडे एकत्रित कराये जायें तथा निर्माण डिजाइन के अनुसार किया जाये। वर्तमान परिदृश्य में भूमिगत जल का सही एवं सम्पूर्ण आंकलन करने, भूमि उपयोग की समस्त जानकारी करने, सिंचित/असिंचित भूमि के आंकलन करने, आदर्श योजना स्थल का चयन करने की दृष्टि से बिना रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस तकनीकी के भूगर्भ जल विभाग की कल्पना अर्थहीन है। भूगर्भ जल के सम्पूर्ण कार्य को करने एवं त्मबींतहम योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि निम्न कार्य करने होंगे।
उत्तराखण्ड राज्य में लगातार भूगर्भीय जल के बढ़ते उपयोग एवं उनके अनियोजित दोहन होने तथा पर्याप्त संग्रहण (रिचार्ज) न होने के कारण भूगर्भीय जल स्तर का लगातार ह्रास हो रहा है। राज्य के 13 जिलों में से 11 जिलों का अधिकांश भूभाग पर्वतीय है। वहाँ पर भी नदी नालों एवं स्रोतों पर लगातार पेयजल एवं सिंचाई आदि की योजनाएं बनाई जा रही है तथा स्रोतों के रिचार्ज हेतु कोई योजना न होने के कारण स्रोतों के श्राव में कमी देखी जा रही है एवं कतिपय स्रोतों के सूखने की सूचना है। राज्य के औद्योगीकरण की बढ़ती सम्भावनाओं को देखते हुए भविष्य में भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने की भी सम्भावना है। यहाँ जल की प्रचुरता होने के बावजूद पेयजल एवं सिंचाई आदि के लिए पानी की हमेशा कमी रही है। भूगर्भीय जल के स्तर में गिरावट तथा पर्वतीय जनपदों के नदी, नालों एवं स्रोतों के श्राव में कमी को दूर करने के लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने, पेयजल, सिंचाई तथा उद्योग आदि के लिए पानी का सुनियोजित उपयोग आवश्यक है।
उत्तराखण्ड राज्य के गठन से पूर्व पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में “भूगर्भ जल विभाग” पृथक रूप से अस्तित्व में था। उत्तरांचल राज्य के मैदानी क्षेत्रों की भूमिगत जल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति इस विभाग द्वारा की जाती थी। इसके लिए मैदानी क्षेत्रों में कई भू-जलस्तर मापक यंत्र/स्थल तथा वर्षा जल मापक यंत्र/स्थल स्थापित है, जिससे आंकड़े एकत्रित कर उपयोग किए जाते हैं। उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आने के बाद इस कार्य हेतु कोई संस्था/विभाग नहीं रह गया था एवं उत्तर प्रदेश द्वारा भी उत्तरांचल क्षेत्र में भूगर्भ जल सम्बन्धी कार्य छोड़ दिया गया है, जिसके कारण भूमिगत जल सम्बन्धी आंकड़े वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित स्थल अच्छे आंकड़ों की पूर्ति नहीं थी, जिसके लिए अतिरिक्त स्टेशन लगाये जाने एवं कर्मचारी लगाये जाने की आवश्यकता होगी।
उत्तरांचल के मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों जहाँ पर नदी नालों एवं स्रोतों के श्राव लगातार कम होते जा रहे हैं, के आंकड़े एकत्र करने के बारे में पूर्व में भी कोई व्यवस्था नहीं थी। समय आ गया है कि इन क्षेत्रों के जलभंड के ह्रास के कारणों का सात्त किया जाये। जगह-जगह पर स्रोतों को चिह्नित कर उसके श्राव का मापन किया जाए एवं तुलनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष कर पहुंचा जाए। नदी नालों पर पेड़ झाड़ियों से पानी को कृत्रिम रूप से रोकने, चाल खाल बनाने की जानकारी जनता को दिया जाना चाहिए।
को खूबू थी। वर्तमान में यह प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है। चाल खाल नष्ट होते जा रहे हैं। नदी नालों के बहाव को जगह-जगह पर रोककर रिचार्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं रह गयी थी। ऐसे में यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम आंकड़े एकत्रित कराये जायें तथा निर्माण डिजाइन के अनुसार किया जाये। वर्तमान परिस्थिति में भूमिगत जल का सही एवं सम्पूर्ण आकलन करने, भूमि उपयोग की समस्त जानकारी करने, सिंचित/असिंचित भूमि के आकलन करने, आदर्श योजना स्थल का चयन करने की दृष्टि से बिना लघुद्यम मद्देपद्र एवं वृह्प तकनीकी के भूगर्भ जल विभाग की कल्पना अपेक्षित है। भूगर्भ जल के सम्पूर्ण कार्य को करने एवं रिचार्ज योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से कार्य करने होंगे।
देश का लगभग 54 प्रतिशत भाग अत्यधिक जल की कमी से ग्रसित है, राज्य के मैदानी जनपदों में भू-जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड, देहरादून कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जल के अत्यधिक दोहन के कारण जल स्तर में गिरावट हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार जनपद हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के 5 विकासखण्ड अति ब्लॉक स्थिति में है, जबकि कुछ अन्य विकासखण्डों में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। लगातार हो रहे पर्यावरणीय कारणों से कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में भी गर्मी के मौसम में पेयजल एवं सिंचाई हेतु पानी की कमी हो जाती है।
लघु सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई के साथ-साथ जल संरक्षण एवं संवर्द्धन का भी कार्य किया जा रहा है। जल संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु विभाग द्वारा लघु योजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है –
1. चेकडैम
विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में चेक डैम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। चेक डैम जहाँ सिंचाई योजनाओं के स्थाई हेड के रूप में कार्य करते हैं जिससे सिंचाई योजनाएं लगातार क्रियाशील रहती हैं वहीं इन योजनाओं से जल संरक्षण एवं संवर्द्धन भी होता है।
चेक डैम निर्माण के लाभ:
- सिंचाई योजनाओं के हेड को स्थायित्व मिलता है एवं वह वर्ष पर्यंत क्रियाशील रहती हैं।
- मृदा कटाव एवं तल क्षरण को रोकने में सहायक हैं।
- जल संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य करता है तथा चेक डेम के ऊपरी भाग में नियमित रूप से जल भराव बना रहता है।
- चेक डेम के आसपास के क्षेत्रों में नमी की मात्रा बढ़ने के कारण गर्मी के मौसम में भी हरियाली होने के कारण वनस्पति से होने वाली हानि की संभावना कम हो जाती है।
- चेक डेम से एकत्रित पानी का उपयोग सिंचाई के अतिरिक्त विभिन्न उद्देश्यों जैसे मछली पालन, पशुओं के पेयजल, पर्यटन, उप्तत घाट को स्थायित्व करने एवं अन्य उपयोगार्थ भी किया जा सकता है।